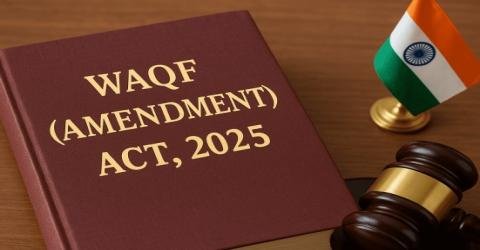क्या भारत का वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 असंवैधानिक है?
भारतीय संसद द्वारा पारित और 8 अप्रैल, 2025 को अधिनियमित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक क्षेत्रों में गहन बहस छेड़ दी है। यह कानून, जो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है, का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है - धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित इस्लामी बंदोबस्ती। हालाँकि, इसके प्रावधानों का काफी विरोध हुआ है, आलोचकों ने इसे असंवैधानिक और धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करार दिया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल, 2025 को कानून को चुनौती देने वाली सुनवाई के लिए तैयार है, सवाल यह है: क्या वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 भारत के संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन करता है?
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की पृष्ठभूमि
वक्फ अधिनियम, 1995 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करता है, जिसका प्रबंधन राज्य और केंद्र की निगरानी में वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित वक्फ संपत्तियां, पैमाने में महत्वपूर्ण हैं, अनुमान है कि भारत भर में लाखों एकड़ में फैली 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं। 2025 का संशोधन इस ढांचे में कई बदलाव पेश करता है, जिसका घोषित लक्ष्य वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है।
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
वक्फ प्रशासन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना: अधिनियम में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का आदेश दिया गया है, आलोचकों का तर्क है कि यह कदम वक्फ प्रशासन के धार्मिक चरित्र को कमजोर करता है।
'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' का उन्मूलन: औपचारिक दस्तावेजीकरण के बिना दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्तियों को मान्यता देने की अवधारणा को हटा दिया गया है, जिससे ऐतिहासिक वक्फ की स्थिति के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
बढ़ाया हुआ राज्य नियंत्रण: अधिनियम जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों पर विवादों को हल करने का अधिकार देता है, वक्फ बोर्डों से अधिकार राज्य राजस्व तंत्र को हस्तांतरित करता है।
पांच वर्षीय मुस्लिम अभ्यास खंड: एक नई आवश्यकता यह निर्धारित करती है कि केवल वे व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का अभ्यास किया है, जिससे इसकी प्रवर्तनीयता और निष्पक्षता के बारे में सवाल उठते हैं।
वक्फ न्यायाधिकरणों में परिवर्तन: न्यायाधिकरण संरचना में अब मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, और अब अपील उच्च न्यायालयों में जा सकती है, जिससे वक्फ विवादों के लिए न्यायिक प्रक्रिया बदल जाती है।
अनिवार्य पंजीकरण और डिजिटलीकरण: सभी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए, जिसका विवरण एक केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, जिससे छोटे या अनिर्दिष्ट वक्फों के लिए तार्किक चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार इस कानून का बचाव एक “ऐतिहासिक सुधार” के रूप में करती है, जिसका उद्देश्य कुप्रबंधन को रोकना और हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों तक लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करना है। राइजिंग भारत समिट 2025 में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गरीब और पसमांदा मुसलमानों के लिए “सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम” कहा। हालाँकि, विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताते हुए तर्क दिया है कि यह अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है।
संवैधानिक चिंताएँ: मुख्य तर्क
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता भारतीय संविधान के कई प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 300A पर निर्भर करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं सहित आलोचकों ने सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएँ दायर की हैं, जिनमें निम्नलिखित आधारों पर कानून को चुनौती दी गई है:
1. धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन (अनुच्छेद 25 और 26)
अनुच्छेद 25 धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने, संस्थाओं की स्थापना करने और अपनी मान्यताओं के अनुसार संपत्तियों का प्रशासन करने का अधिकार देता है। आलोचकों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर-मुसलमानों को शामिल करने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता कम हो जाती है, जो स्वाभाविक रूप से धार्मिक प्रकृति की होती हैं।
आईयूएमएल की याचिका में अधिनियम को "मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों पर असंवैधानिक हमला" बताया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि वक्फ, इस्लामी कानून में निहित एक अवधारणा के रूप में, केवल मुसलमानों द्वारा शासित होना चाहिए। न्यायाधिकरणों में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता को हटाना और विवाद समाधान का काम जिला कलेक्टरों को सौंपना - जो अक्सर गैर-मुस्लिम होते हैं - धार्मिक स्वशासन पर और अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है।
सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियां केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि व्यापक धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराती है। यह कानून के समावेशी इरादे के सबूत के रूप में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समर्थन का हवाला देता है।
2. भेदभाव और समानता (अनुच्छेद 14 और 15)
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। पांच साल की मुस्लिम प्रैक्टिस क्लॉज ने विशेष रूप से जांच की है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक जैसे आलोचकों ने सवाल उठाया है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रैक्टिस को कौन प्रमाणित करेगा। उनका तर्क है कि यह प्रावधान मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो अनुच्छेद 14 की समान व्यवहार की गारंटी का उल्लंघन करता है।
इसके अतिरिक्त, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अधिनियम मुसलमानों को असंगत रूप से लक्षित करता है, यह देखते हुए कि हिंदू बंदोबस्ती या अन्य धार्मिक ट्रस्टों के लिए कोई समान प्रतिबंध मौजूद नहीं हैं। राज्य अधिकारियों, विशेष रूप से जिला कलेक्टरों की बढ़ी हुई भूमिका को मुस्लिम संपत्तियों पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष में देखा जाता है, जो संभावित रूप से अनुच्छेद 15 के भेदभाव-विरोधी जनादेश का उल्लंघन करता है।
सरकार का तर्क है कि यह क्लॉज वक्फ निर्माण में वास्तविक इरादे को सुनिश्चित करता है, गैर-अभ्यास करने वाले व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग को रोकता है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कानून सभी वक्फ संपत्तियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे निर्माता की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इस प्रकार समानता के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है।
3. संपत्ति अधिकार (अनुच्छेद 300ए)
अनुच्छेद 300ए व्यक्तियों को उचित प्रक्रिया के अलावा संपत्ति से वंचित होने से बचाता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम के प्रावधान - जैसे कि 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' को खत्म करना और छह महीने की सीमित अवधि के भीतर अनिवार्य पंजीकरण - ऐतिहासिक वक्फों की स्थिति को खतरे में डालते हैं, जिनमें से कई में औपचारिक कार्य नहीं हैं। वक्फ बोर्ड को दरकिनार करते हुए जिला कलेक्टरों को वक्फ की स्थिति निर्धारित करने का अधिकार हस्तांतरित करना संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करने के रूप में देखा जाता है, जिससे संभावित रूप से वक्फ भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका में चेतावनी दी गई है कि ये बदलाव "कई वक्फ संपत्तियों को असुरक्षित" बना सकते हैं, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हालांकि, सरकार का दावा है कि अधिनियम स्वामित्व को स्पष्ट करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को गलती से वक्फ के रूप में दर्ज किया गया है, इस प्रकार सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा की जाती है।
4. संघवाद और विधायी क्षमता
डीएमके समेत कुछ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले धार्मिक बंदोबस्त के प्रबंधन के लिए राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करके संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है। जिला कलेक्टर जैसे राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बढ़ी हुई भूमिका को केंद्र और राज्य प्राधिकरण के बीच संतुलन को बाधित करने के रूप में देखा जाता है, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जहां अधिनियम का विरोध करने वाले प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
केंद्र ने अपने अधिकार का बचाव करते हुए वक्फ अधिनियम की लंबे समय से केंद्रीय कानून के रूप में स्थिति और देश भर में कुप्रबंधन को दूर करने के लिए समान सुधारों की आवश्यकता का हवाला दिया।
सरकार का बचाव: पारदर्शिता और सामाजिक न्याय
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इस बात पर जोर देती है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे कुप्रबंधन को दूर करने के लिए एक सुधारात्मक उपाय है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्डों में अनियमितताओं को उजागर किया है, उनका दावा है कि संशोधन जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और हाशिए पर पड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाते हैं। सरकार का तर्क है कि गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से विविधता को बढ़ावा मिलता है और बोर्डों के भीतर संभावित पक्षपात की जाँच होती है।
अधिनियम के डिजिटलीकरण अधिदेश का उद्देश्य पारदर्शी डेटाबेस बनाना, विवादों और अवैध अतिक्रमणों को कम करना है। कुप्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और स्थानीय समितियों में दानकर्ता परिवारों के प्रतिनिधित्व के प्रावधानों को जमीनी स्तर के हितधारकों को सशक्त बनाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरकार 17 घंटे की राज्यसभा बहस को भी इंगित करती है - जो उच्च सदन के इतिहास में सबसे लंबी है - विपक्ष के अपर्याप्त परामर्श के दावों के बावजूद गहन विचार-विमर्श का सबूत है।
सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
अधिनियम ने जनता की राय को ध्रुवीकृत कर दिया है। हैदराबाद, कोलकाता और मणिपुर जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें AIMPLB और दर्सगाह-जिहाद-ओ-शहादत जैसे मुस्लिम संगठनों ने इसे "काला कानून" करार दिया। कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित राजनीतिक दलों ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर इसके प्रभाव की आलोचना की है। इसके विपरीत, भाजपा के सहयोगी दलों और कुछ सामुदायिक आवाज़ों ने पारदर्शिता और समावेशिता के लाभों का हवाला देते हुए सुधारों का स्वागत किया है।
आगे की राह: सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
16 अप्रैल, 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच के समक्ष सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई निर्णायक होगी। अधिनियम को चुनौती देने वाली 10 से अधिक याचिकाओं के साथ, न्यायालय यह आकलन करेगा कि इसके प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या राज्य की नियामक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। किसी भी आदेश से पहले सुनवाई की मांग करने वाली केंद्र की चेतावनी, उच्च दांव को रेखांकित करती है।
कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि न्यायालय सार्वजनिक संपत्तियों को विनियमित करने में राज्य के हित के साथ धार्मिक स्वायत्तता को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। धार्मिक संपत्ति अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले जैसे उदाहरण, जिसमें 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' को मान्यता दी गई थी, परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम रोक, अधिनियम के प्रवर्तन को रोक सकती है, लेकिन तत्काल सुनवाई देने के लिए न्यायालय की अनिच्छा एक मापा दृष्टिकोण का सुझाव देती है।
निष्कर्ष: एक संवैधानिक पेंच
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और राज्य प्राधिकरण के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। जबकि सरकार इसे पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के लिए एक सुधार के रूप में पेश करती है, आलोचक इसे एक अतिक्रमण के रूप में देखते हैं जो मुस्लिम स्वायत्तता और संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करता है। अधिनियम असंवैधानिक है या नहीं यह अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 300A पर इसके प्रभाव की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर करेगा।
जबकि भारत न्यायपालिका के फैसले का इंतजार कर रहा है, बहस धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक मामलों में राज्य की भूमिका के बारे में गहरे तनाव को रेखांकित करती है। परिणाम न केवल वक्फ संपत्तियों के भविष्य को आकार देगा बल्कि एक ध्रुवीकृत परिदृश्य में भारत विविधता और शासन को कैसे संतुलित करता है, इसके लिए एक मिसाल भी स्थापित करेगा।
स्रोत:
द हिंदू, “वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध”
बिजनेस स्टैंडर्ड, “वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा”
एनडीटीवी, “वक्फ अधिनियम लागू हुआ, शीर्ष अदालत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी”
लाइवलॉ, “वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली आईयूएमएल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया”
इंडिया टुडे, “नए वक्फ कानून में 5 साल का मुस्लिम क्लॉज क्यों है”
सार्वजनिक और राजनीतिक भावना को दर्शाते हुए एक्स पर पोस्ट