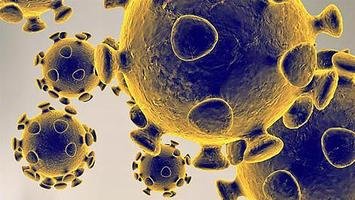इस वक़्त पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की गिरफ़्त में कराह रही है। इसके लिए नया कोरोना वायरस या SARS CoV-2 जिम्मेदार है। मानवता पर कहर बरपाने वाला ये पहला वायरस नहीं है। विषाणुओं ने कई बार मानवता को भयंकर चोट पहुंचाई है।
1918 में दुनिया पर कहर ढाने वाले इन्फ्लुएंज़ा वायरस से पांच से दस करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसा अनुमान है कि बीसवीं सदी में चेचक के वायरस ने कम से कम बीस करोड़ लोगों की जान ले ली है।
इन उदाहरणों को देख कर यही लगता है कि वायरस हमारे लिए बड़ा ख़तरा हैं और इनका धरती से ख़ात्मा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि धरती से सारे विषाणुओं का सफ़ाया हो जाये।
लेकिन, वायरस को धरती से विलुप्त कर देने का इरादा करने से पहले सावधान हो जाइए। अगर ऐसा हुआ, तो हम भी नहीं बचेंगे। बिना वायरस के इंसान ही नहीं, इस धरती में जीवन का अस्तित्व मुमकिन नहीं है।
अमरीका की विस्कॉन्सिन-मेडिसन यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ टोनी गोल्डबर्ग कहते हैं, ''अगर अचानक धरती से सारे वायरस ख़त्म हो जाएंगे, तो इस धरती के सभी जीवों को मरने में बस एक से डेढ़ दिन का वक़्त लगेगा। वायरस इस धरती पर जीवन को चलाने की धुरी हैं। इसलिए हमें उनकी बुराइयों की अनदेखी करनी होगी।''
दुनिया में कितने तरह के वायरस हैं, इसका अभी पता नहीं है। पता है तो बस ये बात कि ये ज़्यादातर विषाणु इंसानों में कोई रोग नहीं फैलाते। हज़ारों वायरस ऐसे हैं, जो इस धरती का इकोसिस्टम चलाने में बेहद अहम रोल निभाते हैं। फिर चाहे वो कीड़े-मकोड़े हों, गाय-भैंस या फिर इंसान।
मेक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी की वायरस विशेषज्ञ सुसाना लोपेज़ शैरेटन कहती हैं कि, "इस धरती पर वायरस और बाक़ी जीव पूरी तरह संतुलित वातावरण में रहते हैं। बिना वायरस के हम नहीं बचेंगे।''
ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि वायरस इस धरती पर जीवन को चलाने के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इसकी एक वजह ये है कि हम केवल उन्हीं वायरसों के बारे में रिसर्च करते हैं, जिनसे बीमारियां होती हैं। हालांकि अब कुछ साहसी वैज्ञानिकों ने वायरस की अनजानी दुनिया की ओर क़दम बढ़ाया है।
अब तक केवल कुछ हज़ार वायरसों का पता इंसान को है जबकि करोड़ों की संख्या में ऐसे वायरस हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। पेन्सिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की मैरिलिन रूसिंक कहती हैं कि, ''विज्ञान केवल रोगाणुओं का अध्ययन करता है। ये अफ़सोस की बात है। मगर सच यही है।''
अब चूंकि ज़्यादातर वायरसों के बारे में हमें पता ही नहीं, तो ये भी नहीं पता कि कितने वायरस इंसान के लिए ख़तरनाक हैं। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विषाणु वैज्ञानिक कर्टिस सटल कहते हैं कि, "अगर वायरस प्रजातियों की कुल संख्या के हिसाब से देखें, तो इंसान के लिए ख़तरनाक विषाणुओं की संख्या शून्य के आस पास होगी।''
वायरस इकोसिस्टम की धुरी हैं। हमारे लिए वो वायरस सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इन्हें फेगस कहते हैं। जिसका अर्थ है निगल जाने वाले।
टोनी गोल्डबर्ग कहते हैं कि समंदर में बैक्टीरिया की आबादी नियंत्रित करने में फेगस विषाणुओं का बेहद अहम रोल है। अगर ये वायरस ख़त्म हो जाते हैं, तो अचानक से समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा।
समुद्र में 90 फ़ीसद जीव, माइक्रोब यानी छोटे एक कोशिकाओं वाले जीव हैं। ये धरती की आधी ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये काम वायरस के बिना नहीं हो सकता। समंदर में पाए जाने वाले वायरस वहां के आधे बैक्टीरिया और 20 प्रतिशत माइक्रोब्स को हर रोज़ मार देते हैं।
इससे, समुद्र में मौजूद काई, शैवाल और दूसरी वनस्पतियों को ख़ुराक मिलती है। जिससे वो फोटो सिंथेसिस करके, सूरज की रौशनी की मदद से ऑक्सीजन बनाते हैं। और इसी ऑक्सीजन से धरती पर ज़िंदगी चलती है। अगर वायरस ख़त्म हो जाएंगे, तो समुद्र में इतनी ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी। फिर पृथ्वी पर जीवन नहीं चल सकेगा।
कर्टिस सटल कहते हैं कि, ''अगर मौत न हो, तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं। क्योंकि ज़िंदगी, धरती पर मौजूद तत्वों की रिसाइकिलिंग पर निर्भर करती है। और इस रिसाइकिलिंग को वायरस करते हैं।''
दुनिया में जीवों की आबादी कंट्रोल करने के लिए भी वायरस ज़रूरी हैं। जब भी किसी जीव की आबादी बढ़ती है, तो विषाणु उस पर हमला करके आबादी को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि महामारियों के ज़रिए इंसान की आबादी नियंत्रित होती है। वायरस न होंगे, तो धरती पर जीवों की आबादी आउट ऑफ़ कंट्रोल हो जाएगी। एक ही प्रजाति का बोलबाला होगा, तो जैव विविधता समाप्त हो जाएगी।
कुछ जीवों का तो अस्तित्व ही वायरसों पर निर्भर है। जैसे कि गायें और जुगाली करने वाले दूसरे जीव। वायरस इन जीवों को घास के सेल्यूलोज़ को शुगर में तब्दील करने में मदद करते हैं। और फिर यही उनके शरीर पर मांस चढ़ने और उनके दूध देने का स्रोत बनती है।
इंसानों और दूसरे जीवों के भीतर पल रहे बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में भी वायरस का बड़ा योगदान होता है।
अमरीका के मशहूर यलोस्टोन नेशनल पार्क की घास भयंकर गर्मी बर्दाश्त कर पाती है, तो इसके पीछे वायरस का ही योगदान है। ये बात रूसिंक और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च से साबित की है।
हलापेनो के बीज में पाए जाने वाले वायरस इसे उन कीड़ों से बचाते हैं, जो पौधों का रस सोखते हैं। रूसिंक की टीम ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कुछ पौधे और फफूंद, वायरस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते जाते हैं, ताकि उनका सुरक्षा चक्र बना रहे। अगर वायरस फ़ायदेमंद न होते, तो पौधे ऐसा क्यों करते?
वायरस इंसानों का सुरक्षा चक्र बनाते हैं। कई वायरस का संक्रमण हमें ख़ास तरह के रोगाणुओं से बचाता है। डेंगू के लिए ज़िम्मेदार वायरस का एक दूर का रिश्तेदार GB वायरस C एक ऐसा ही वायरस है। इससे संक्रमित व्यक्ति में एड्स की बीमारी तेज़ी से नहीं फैलती। और अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में है, तो उसके इबोला वायरस से मरने की आशंका कम हो जाती है।
हर्पीज़ वायरस हमें प्लेग और लिस्टेरिया नाम की बीमारियों से बचा सकता है। हर्पीज़ के शिकार चूहे, इन बीमारियों के बैक्टीरिया से बच जाते हैं।
वायरस हमारे कई बीमारियों से लड़ने की दवा भी बन सकते हैं। 1920 के दशक में सोवियत संघ में इस दिशा में काफ़ी रिसर्च हुई थी। अब दुनिया में कई वैज्ञानिक फिर से वायरस थेरेपी पर रिसर्च कर रहे हैं। जिस तरह से बैक्टीरिया, एंटी बायोटिक से इम्यून हो रहे हैं, तो हमें जल्द ही एंटी बायोटिक का विकल्प तलाशना होगा। वायरस ये काम कर सकते हैं। वो रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या कैंसर कोशिकाओं का ख़ात्मा करने में काम आ सकते हैं।
कर्टिस सटल कहते हैं कि, "इन रोगों से लड़ने के लिए हम वायरस को ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई गाइडेड मिसाइल हो। जो सीधे लक्ष्य पर यानी नुक़सानदेह रोगाणुओं पर निशाना लगाएंगे, बैक्टीरिया या कैंसर की कोशिकाओं का ख़ात्मा कर देंगे। वायरस के ज़रिए हम तमाम रोगों के इलाज की नई पीढ़ी की दवाएं तैयार कर सकते हैं।''
चूंकि वायरस लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इनके पास जेनेटिक जानकारी का ख़ज़ाना होता है। ये दूसरी कोशिकाओं में घुस कर अपने जीन को कॉपी करने के सिस्टम पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं। इसलिए, इन वायरस का जेनेटिक कोड हमेशा के लिए उस जीव की कोशिका में दर्ज हो जाता है।
हम इंसानों के आठ प्रतिशत जीन भी वायरस से ही मिले हैं। 2018 में वैज्ञानिकों की दो टीमों ने पता लगाया था कि करोड़ों साल पहले वायरस से हमें मिले कोड हमारी याददाश्त को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
अगर, आज इंसान अंडे देने के बजाय सीधे बच्चे को जन्म दे पाते हैं, तो ये भी एक वायरस के इन्फ़ेक्शन का ही कमाल है। आज से क़रीब 13 करोड़ साल पहले इंसान के पूर्वजों में रेट्रोवायरस का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला था। उस संक्रमण से इंसानों की कोशिकाओं में आए एक जीन के कारण ही, इंसानों में गर्भ धारण और फिर अंडे देने के बजाय सीधे बच्चा पैदा करने की ख़ूबी विकसित हुई।
धरती पर वायरस ये जो तमाम भूमिकाएं निभा रहे हैं, उनके बारे में अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू ही की हैं। हम जैसे-जैसे इनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, तो हम वायरस का और बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। शायद उनसे हमें कई बीमारियों से लड़ने का ज़रिया मिले या अन्य ऐसी मदद मिले, जिससे इंसानियत ही नहीं, पूरी धरती का भला हो। इसलिए वायरस से नफ़रत करने के बजाय उनके बारे में और जानने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए।